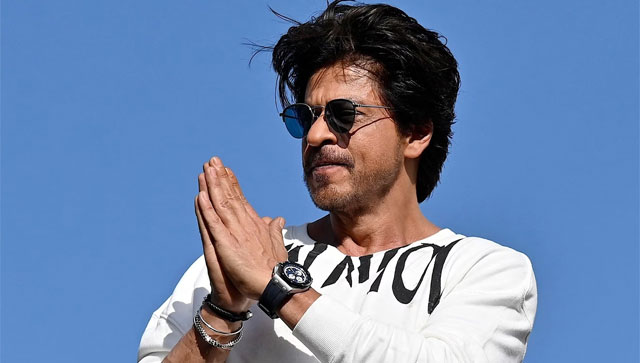तमिल सेल्युलाइड उद्योग और द्रविड़ राजनीति के बीच हमेशा एक दीर्घकालिक वैवाहिक संबंध रहा है। सिनेमा लामबंदी और राजनीतिक प्रचार के लिए द्रविड़ पार्टियों की नाभि रही है। कई नेताओं और मुख्यमंत्रियों ने सेल्युलाइड दुनिया की अपनी छवियों के आधार पर नागरिकों को वोट देने की क्षमता विकसित की है। जैसा कि तमिल फिल्म इतिहासकार थोडोर बस्करन ने कहा, फिल्में राजनीतिक दलों के जन अभियानों का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।
अपने शुरुआती दिनों में द्रविड़ पार्टियों का ध्यान गैर-ब्राह्मण आंदोलनों, स्वाभिमान, लोकतंत्र और समानता पर था। हालाँकि तमिल फिल्में सामाजिक सुधारों से संबंधित कई समान विषयों से निपटती हैं, फिर भी गैर-ब्राह्मणों और दलितों के बीच जाति संघर्ष की पूरी गहराई से जांच की जानी बाकी है। हालिया फिल्म मामन्नान प्रमुख द्रविड़ राजनीतिक दलों के भीतर दलितों की स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रयास था।
वर्तमान पार्टियों का प्रतिबिंब?
मारी सेल्वराज की तीसरी फिल्म मामन्नान इसे कई सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं और इसने जातिवाद पर अंतर-पार्टी द्वंद्वात्मकता पर बहुस्तरीय चर्चा उत्पन्न की है। फिल्म के नायक – मामनन के रूप में वाडिवेलु, अथिवीरन के रूप में उदयनिधि स्टालिन, लीला के रूप में कीर्ति सुरेश और रत्नावेलु के रूप में फहद फाजिल – तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियों के भीतर जातिवाद की वस्तुनिष्ठ स्थिति को चित्रित करते हैं। यह जाति के उन्मूलन या कम से कम वैचारिक अभिविन्यास के माध्यम से अपने नेताओं और कैडरों के बीच अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म करने की दिशा में रास्ता तैयार करने में द्रविड़ पार्टियों की कमजोरी को उजागर करता है।
फिल्म ने जनता के साथ-साथ राजनीतिक हलकों में भी बहस और चर्चा पैदा कर दी है। यह दलित समुदाय से आने वाले अपने सहयोगियों के प्रति द्रविड़ पार्टी के नेताओं के व्यवहार के बारे में छिपी सच्चाई को उजागर करता है। हालाँकि इस वास्तविकता के बारे में कुछ तमिल साहित्यिक कथाओं में वर्णन किया गया है, विशेष रूप से इमायम, पेरुमल मुरुगन, शिवगामी और अन्य जैसे लेखकों द्वारा, इस फिल्म ने जनता के बीच ऐसी चर्चाएं शुरू कर दी हैं। यह वास्तव में फिल्म की बड़ी सफलता है।
कुछ लोगों ने फिल्म की पहचान ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पी. धनपाल के अनुभव से की है, जबकि कुछ अन्य लोगों में फिल्म ने थोल की यादें ताजा कर दीं। संसद सदस्य और विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) के अध्यक्ष तिरुमावलवन को चिदंबरम निर्वाचन क्षेत्र के कुछ गांवों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया, जहां से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था। इसके अलावा, कुछ लोग यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि क्या फिल्म में मुख्य जातीय हिंदू चरित्र अन्नाद्रमुक का एक वरिष्ठ नेता है।
प्रमुख विषय
फिल्म में कुछ स्थितियों को संवाद के माध्यम से मार्मिक ढंग से दर्शाया गया है जैसे कि अपने जाति हिंदू गुरु सलेम सुंदरम के संबंध में मामनन की बेबसी। बाद में, रत्नावेलु और अथिवीरन के बीच एक-दूसरे के बराबर बैठने को लेकर तीखी बहस, जारी आधिपत्यवादी जाति प्रथाओं के सामने आत्म-सम्मान के दावे में बदल जाती है। रत्नावेलु अथिवीरन को बताता है कि उसने उसे अपने साथ बैठने के लिए सीट की पेशकश इसलिए की क्योंकि वह उसकी राजनीति है (अरासियाल) जबकि वही प्रस्ताव अथिवीरन के पिता को उनकी अपनी प्रमुख जाति हिंदू पहचान के कारण नहीं दिया गया है (अदयालम). तमिल सिनेमा के लिए ऐसा साहसपूर्वक ऐसा अनुक्रम दिखाना दुर्लभ है जो जाति की राजनीति की रोजमर्रा की प्रकृति को दर्शाता है। इसी तरह, फिल्म आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों, दलित राजनीतिक प्रतिनिधियों और कैसे और क्यों जाति के हिंदू नेता दलित आत्म-पुष्टि को नियंत्रित करने के लिए दलित नेताओं को निवेश और तैयार करते हैं, के बारे में बातचीत करती है। व्यावसायिक सिनेमा में नग्न जाति की राजनीति का आग्रहपूर्वक चित्रण करने के लिए निर्देशक और अभिनेता हमारी सराहना के पात्र हैं।
फिल्म इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे ‘जातीय गौरव’ के लिए जातिवादी हिंदू नेता हिंसा या हत्या के जरिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये उदाहरण दर्शकों को राज्य में लंबे समय से चल रही जातीय हत्याओं की याद दिलाते हैं। इसके अतिरिक्त, मारी सेल्वराज जातिवादी समाज में नाम पुकारने की राजनीति को पकड़ती है। वह उजागर करता है कि कैसे साथी जाति के हिंदू नेता दलित नेता ममन्नान को संबोधित करते हैं मानु मतलब मिट्टी, (अपमानजनक तरीके से) इसे स्नेह के बहाने छिपाकर। केवल उनका बेटा अथिवीरन ही उन्हें उनके पूरे नाम से बुलाता है।
इस फिल्म में महिलाओं का चित्रण भी बोधगम्य है। विशेष रूप से, ममन्नान की पत्नी, वीरायी और रत्नावेलु की पत्नी, जोथी की आंखें बहुत कुछ कहती हैं।
कोंगु क्षेत्र में जाति
अतीत में, कुछ फिल्में पसंद आईं मुथल वसंतम, चिन्ना थम्बी पेरिया थम्बी और चिन्ना गौंडर पश्चिमी तमिलनाडु के जातिवाद का चित्रण किया है। ये फिल्में या तो व्यंग्यात्मक थीं या कोंगु क्षेत्र में प्रचलित सामंती व्यवस्था का महिमामंडन करती थीं। वास्तव में, अन्य क्षेत्रों – तमिलनाडु के दक्षिण या उत्तर – के विपरीत, पश्चिमी क्षेत्र में जातिवादी कट्टरपंथी हैं, जो राजनीति के क्षेत्र से बाहर अन्य क्षेत्रों में सक्रिय हैं। यह सर्वविदित है कि इस क्षेत्र में विशाल राजनीतिक शक्ति के साथ-साथ उच्च जाति के हिंदू भूमि, व्यवसायों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी पदों के स्वामित्व पर एकाधिकार रखते हैं। सवर्ण हिंदुओं और दलितों के बीच असमानता बहुत बड़ी है और उन्हें चुनौती देना आसान नहीं है। वास्तव में, कोंगु क्षेत्र जातीय हिंदू वर्चस्व का प्रतीक है।
इसके अतिरिक्त, सलेम, नमक्कल, धर्मपुरी, इरोड, करूर और कोवई अपने विभिन्न आवासीय निजी शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाने जाते हैं, जो ज्यादातर जाति के हिंदुओं के स्वामित्व में हैं, जिन्हें पेरुमल मुरागन ने एक बार “पोल्ट्री स्कूल” कहा था। इसलिए, यह कोई रहस्य नहीं है कि निदेशक ने मुफ्त कोचिंग सेंटरों और निजी वाणिज्यिक संस्थानों को केंद्रीय संघर्ष क्यों बनाया। दरार तब शुरू होती है जब लीला और उसके दोस्त गरीब छात्रों के लिए एक मुफ्त कोचिंग सेंटर चलाने लगते हैं जिसे निजी व्यावसायिक संस्थानों के लिए हानिकारक माना जाता है।
भले ही विभिन्न शोधकर्ताओं ने द्रविड़ पार्टियों के भीतर दलितों की स्थिति और उन्हें जिस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उसका पता लगाया है, फिल्म माध्यम ने इस क्षेत्र को अपनी पूरी क्षमता से नहीं खोजा है। जैसा कि ह्यूगो गोरिंगे ने अपनी पुस्तक में प्रकाश डाला है अछूत नागरिक: तमिलनाडु में दलित आंदोलन और लोकतंत्रीकरण1960 के दशक के भूमि सुधार और अन्य सामाजिक सुधारों से मुख्य रूप से मध्यवर्ती जाति को लाभ हुआ।
के रूप में स्थानिक पृथक्करण की निरंतरता चेरी (मलिन बस्तियां), मंदिरों, श्मशान, भूमि और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं जैसे सामाजिक क्षेत्रों तक पहुंच से इनकार करना अभी भी ठोस हस्तक्षेप के बिना जारी है। गोरिंगे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2001 के चुनावों में, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) कैडर जमीनी स्तर पर दलित पैंथर ऑफ इंडिया पार्टी का समर्थन करने से दूर रहे, भले ही वह डीएमके प्रतीक के तहत खड़ी थी।
प्रख्यात द्रविड़ राजनीति विशेषज्ञ दिवंगत एमएसएस पांडियन ने कहा कि तमिलनाडु में दलित डीएमके राजनेताओं को ऐसे लोग मानते हैं जिन्होंने उन्हें धोखा दिया। मामन्नान पार्टी के भीतर सवर्ण हिंदुओं और दलितों के बीच इस राजनीतिक घमासान को पूरी तरह से उजागर करता है।
आशा की एक किरण
फिल्म सकारात्मक संदेश भी दर्ज करती है। दलितों को अपने भय मनोविकार और दब्बू रवैये से बाहर आना चाहिए। उन्हें आत्मसम्मान कायम रखते हुए अपमान का विरोध करना सीखना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए उन्हें मार्शल आर्ट और अनुशासन सीखना चाहिए।
इसके अलावा, फिल्म यह बात समझाने में सक्षम है कि जातिगत कठोरता के बावजूद अभी भी उम्मीद बाकी है। वे ऐसे लोग हैं जो ऐसी कठोर सीमाओं को पार करते हैं और वास्तविक नेतृत्व का समर्थन करते हैं जो सभी बाधाओं के बीच ममन्नन की जीत की ओर ले जाता है। फिल्म दिखाती है कि भविष्य के लिए बिल्कुल अलग तरह की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए अभी भी जगह और गुंजाइश है।
नायक की भूमिका निभा रहे द्रमुक के राजनीतिक उत्तराधिकारी ने उम्मीद जगाई है कि द्रविड़ राजनीति के भीतर जाति-आधारित भेदभाव की स्वीकार्यता से द्रविड़ आंदोलन के भीतर समानता और न्याय के संस्थापक सिद्धांतों की पुष्टि में अधिक हस्तक्षेप होगा। लेकिन द्रविड़ पार्टियों के भीतर इतना आमूल-चूल सुधार लाना इतना आसान नहीं है. फिल्म ने उम्मीद बरकरार रखी है, लेकिन इसे साकार करना एक कठिन यात्रा होगी।